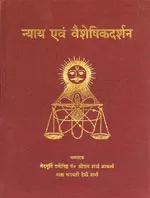|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> न्याय एवं वैशेषिक दर्शन न्याय एवं वैशेषिक दर्शनश्रीराम शर्मा आचार्य
|
256 पाठक हैं |
||||||
न्याय एवं वैशेषिक दर्शन....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
जिन्होंने महर्षि गौतम और कणाद की तरह न्याय एवं वैशेषिक धाराओं का सम्यक्
दर्शन किया, अपनी अनुपम मेधा से पदार्थ-विज्ञान को अध्यात्म-विज्ञान का
पूरक बनाकर ‘वैशेषिक’ को युगानुकूल साक्ष्य देकर
लौकिक जीवन
में अभ्युदय का तथा विचार-विज्ञान को भाव-विज्ञान का सहयोगी बनाकर
‘न्याय’ को युगानुकूल दिशा देकर परम नि:श्रेयस का
मार्ग जन-जन
के लिए प्रशस्त किया।
जिनके द्वारा प्रदत्त चेतन ज्ञान सूत्रों के सहारे ‘न्याय एवं वैशेषिक दर्शन’ का यह नवीन संयुक्त संस्करण संभव हुआ, उन्हीं ऋषियुग्म के श्रीचरणों में यह पुष्प श्रद्धा सहित समर्पित है।
जिनके द्वारा प्रदत्त चेतन ज्ञान सूत्रों के सहारे ‘न्याय एवं वैशेषिक दर्शन’ का यह नवीन संयुक्त संस्करण संभव हुआ, उन्हीं ऋषियुग्म के श्रीचरणों में यह पुष्प श्रद्धा सहित समर्पित है।
नव्यं संस्करणं यस्य कृपादृष्टया प्रकाशितम्।
न्यायं वैशेषिकञ्चैतत् तस्मा एव समर्पितम्।।
न्यायं वैशेषिकञ्चैतत् तस्मा एव समर्पितम्।।
प्रकाशकीय
युगऋषि ने आर्षग्रन्थों के दुर्लभ ज्ञान को जन सुलभ बनाने का
‘‘श्रद्धा-प्रज्ञा’’ युक्त जो
पुरुषार्थ प्रारंभ
किया था; उसी क्रम में शान्तिकुंज में, उन्हीं के अनुशासन एवं मार्गदर्शन
में, उनके ही द्वारा स्थापित वेद-विभाग अपनी अकिंचन शक्ति के साथ
कर्त्तव्यरत है। ऋषियुग्म के निर्देश सूत्रों के आधार पर क्रमश: चार वेद,
108 उपनिषद आदि के नवीन संस्करण के प्रकाशित होने के बाद षड्दर्शनों के
नवीन संस्करणों के प्रकाशन का क्रम बना। उस प्रयास के प्रथम पुष्प के रूप
में ‘सांख्य एवं योगदर्शन’ का संयुक्त संस्करण पाठकों
तक
पहुँचाया जा चुका है। अब उसके द्वितीय पुष्प के रूप में ‘न्याय
एवं
वैशेषिक दर्शन’ का यह संयुक्त संस्मरण प्रस्तुत किया जा रहा है।
पूर्व की भाँति, इस संस्करण का मूल आधार उनके द्वारा प्राकशित मूल संस्करण तथा उनके द्वारा दिए गए सामाजिक निर्देश सूत्रों को ही रखा गया है। उन निर्देशों के अनुसार ही दार्शनिक अभिव्यक्तियों को अधिक स्पष्ट एवं अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उक्त दर्शन ग्रन्थों के संदर्भ में विभिन्न विज्ञ-पुरुषों को विचारों और शोध प्रबन्धों का भी सहयोग लिया गया है। मूल संस्करणों में उनके द्वारा लिखी गई भूमिकाओं की विषय वस्तु को ही उपयुक्त उप शीर्षकों में उभारने वाली शंकाओं एवं विसंगतियों के समुचित समाधान भी जिज्ञासुओं तक पहुँचाने का प्रयास इस संस्करण के माध्यम से किया गया है।
अध्येताओं की सुविधा के लिए इन दर्शनों में प्रयुक्त सूत्रों एवं महत्त्वपूर्ण शब्दों की अनुक्रमणिका भी परिशिष्ट के रूप में जोड़ दी गई है। आशा है कि द्रष्टाओं-ऋषियों की जीवन दृष्टि से विभिन्न पहलुओं को युगानुरूप धारा में जोड़ने के युगऋषि के सत्पुरुषार्थ का समुचित लाभ स्वाध्यायशीलों एवं जिज्ञासुओं तक इस विभाग तक विनम्र प्रयास द्वारा पहुँचाया जा सकेगा।
पूर्व की भाँति, इस संस्करण का मूल आधार उनके द्वारा प्राकशित मूल संस्करण तथा उनके द्वारा दिए गए सामाजिक निर्देश सूत्रों को ही रखा गया है। उन निर्देशों के अनुसार ही दार्शनिक अभिव्यक्तियों को अधिक स्पष्ट एवं अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उक्त दर्शन ग्रन्थों के संदर्भ में विभिन्न विज्ञ-पुरुषों को विचारों और शोध प्रबन्धों का भी सहयोग लिया गया है। मूल संस्करणों में उनके द्वारा लिखी गई भूमिकाओं की विषय वस्तु को ही उपयुक्त उप शीर्षकों में उभारने वाली शंकाओं एवं विसंगतियों के समुचित समाधान भी जिज्ञासुओं तक पहुँचाने का प्रयास इस संस्करण के माध्यम से किया गया है।
अध्येताओं की सुविधा के लिए इन दर्शनों में प्रयुक्त सूत्रों एवं महत्त्वपूर्ण शब्दों की अनुक्रमणिका भी परिशिष्ट के रूप में जोड़ दी गई है। आशा है कि द्रष्टाओं-ऋषियों की जीवन दृष्टि से विभिन्न पहलुओं को युगानुरूप धारा में जोड़ने के युगऋषि के सत्पुरुषार्थ का समुचित लाभ स्वाध्यायशीलों एवं जिज्ञासुओं तक इस विभाग तक विनम्र प्रयास द्वारा पहुँचाया जा सकेगा।
भूमिका
न्यायदर्शन की पृष्ठभूमि
मानव जीवन का लक्ष्य एवं सांसारिक स्थिति में विवेचना अनुभवों के आधार पर
करने वाला न्यायदर्शन, वस्तुवाद का पोषक है। इसके अनुसार जीवन का परम
लक्ष्य मोक्ष है, जिसके द्वारा दु:खों की पूर्णत: निवृत्ति हो जाती है।
न्याय के मतानुसार जीवात्मा कर्त्ता एवं भोक्ता होने के साथ-साथ, ज्ञानादि
से सम्पन्न नित्य तत्त्व है। यह जहाँ वस्तुवाद को मान्यता देता है, वहीं
यथार्थवाद का भी पूरी तरह अनुगमन करता है। मानव जीवन में सुखों की
प्राप्ति का उतना अधिक महत्त्व नहीं है, जितना कि दु:खों की निवृत्ति का।
ज्ञानवान् हो या अज्ञानी, हर छोटा बड़ा व्यक्ति सदैव सुख प्राप्ति का
प्रयत्न करता ही रहता है। सभी चाहते हैं कि उन्हें सदा सुख ही मिले, कभी
दु:खों का सामना न करना पड़े, उनकी समस्त अभिलाषायें पूर्ण होती रहें,
परन्तु ऐसा होता नहीं। अपने आप को पूर्णत: सुखी कदाचित् ही कोई अनुभव करता
हो।
जिनको भरपेट भोजन, तक ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र तथा रहने के लिए मकान भी ठीक से उपलब्ध नहीं तथा दिन भर रोजी-रोटी के लिए मारे मारे फिरते हैं, उनकी कौन कहे; जिनके पास पर्याप्त धन-साधन, श्रेय-सम्मान सब कुछ है, वे भी अपने दु:खों का रोना रोते देखे जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है ? क्या कारण है कि मनुष्य चाहता तो सुख है; किन्तु मिलता उसे दु:ख है। सुख-संतोष के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हुए भी वह अनेकानेक दु:खों एवं अभावों को प्राप्त होता रहता है। आज की वैज्ञानिक समुन्नति से, पहले की अपेक्षा कई गुना सुख के साधनों में बढ़ोत्तरी होने के उपरान्त भी स्थायी समाधान क्यों नहीं मिल सका ? जहाँ साधन विकसित हुए वहीं जटिल समस्याओं का प्रादुर्भाव भी हुआ। मनुष्य शान्ति-संतोष की कमी अनुभव करते हुए चिन्ताग्रस्त एवं दु:खी ही बना रहा। यही कारण है कि मानव जीवन में प्रसन्नता का सतत अभाव होता जा रहा है।
इन समस्त दु:खों एवं अभावों से मनुष्य किस प्रकार मुक्ति पा सकता है, प्राचीन ऋषियों-मनीषियों एवं भारतीय तत्त्वदर्शी महापुरुषों ने इसके लिए कई प्रकार के मार्गों का कथन किया है, जो प्रत्यक्ष रूप से भले ही प्रतिकूल व पृथक् प्रतीत होते हों; परन्तु पात्र व रुचि के आधार पर सबका- अपना-अपना सच्चा दृष्टिकोण है। एक मार्ग वह है जो आत्मस्वरूप के ज्ञान के साथ-साथ भौतिक जगत् के समस्त पदार्थों के प्रति आत्मबुद्धि का भाव रखते हुए पारलौकिक साधनों का उपदेश देता है। दूसरा मार्ग वह है जो जीवमात्र को ईश्वर का अंश बतलाकर, जीवन में सेवा व भक्तिभाव के समावेश से लाभान्वित होकर आत्मलाभ की बात बतलाता है। तीसरा मार्ग वह है जो सांसारिक पदार्थों एवं लौकिक घटनाक्रमों के प्रति सात्विकता पूर्ण दृष्टि रखते हुए, उनके प्रति असक्ति न होने को श्रेयस्कर बताता है।
इसी तीसरे मार्ग का अवलम्बन न्यायदर्शन करता है, जबकि वह ईश्वरोपासना, पुनर्जन्म, लोक-परलोक, आत्मा आदि में भी भरपूर आस्था रखने वाली है, फिर भी इन सबकी सम्यक् उपलब्धि तथा इहलौकिक एवं परलौकिक जीवन की सफलता हेतु भौतिक जगत् के पदार्थों एवं उससे संबंधित घटनाओं का कथन करता है। न्याय का मानना है कि जो भी ज्ञान मनुष्य को उपलब्ध है, वह इन्द्रियों व मन-बुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त हुआ करता है। इन सबमें विकृति उत्पन्न होने की स्थिति में उपलब्ध ज्ञान भी उसी अनुपात में विकारयुक्त हो जाने के कारण उस विकृत ज्ञान का आधार लेकर जो भी निर्णय लिया जायेगा तथा उससे किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति नहीं की जा सकेगी। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायशास्त्र ने यह सैद्धान्तिक अभिव्यक्ति की है कि संसार में न आने के पश्चात् यदि मनुष्य सत्कर्म व सद्व्यवहार के माध्यम से अपने दु:खों को दूर करना चाहे, तो सांसारिक संरचना में प्रयुक्त होने वाले जड़-चेतन सभी पदार्थों का वास्तविक स्वरूप भी जाने समझे। अनेक तरह के मतानुयायियों ने अपने अपने विचार से पदार्थों का स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार का बतलाया है, जिसके कारण मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। इस भ्रमात्मकतापूर्ण स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए न्यायशास्त्र ने तर्क व साक्ष्यों की ऐसी सुन्दर विचारधारा प्रस्तुत की है, जिससे पदार्थों के सही स्वरूप का निर्णय किया जा सके।
जिन साधनों से हमें ज्ञेय तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हीं साधनों को ‘न्याय’ की संज्ञा दी गई है। कहा भी है कि-
जिनको भरपेट भोजन, तक ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र तथा रहने के लिए मकान भी ठीक से उपलब्ध नहीं तथा दिन भर रोजी-रोटी के लिए मारे मारे फिरते हैं, उनकी कौन कहे; जिनके पास पर्याप्त धन-साधन, श्रेय-सम्मान सब कुछ है, वे भी अपने दु:खों का रोना रोते देखे जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है ? क्या कारण है कि मनुष्य चाहता तो सुख है; किन्तु मिलता उसे दु:ख है। सुख-संतोष के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हुए भी वह अनेकानेक दु:खों एवं अभावों को प्राप्त होता रहता है। आज की वैज्ञानिक समुन्नति से, पहले की अपेक्षा कई गुना सुख के साधनों में बढ़ोत्तरी होने के उपरान्त भी स्थायी समाधान क्यों नहीं मिल सका ? जहाँ साधन विकसित हुए वहीं जटिल समस्याओं का प्रादुर्भाव भी हुआ। मनुष्य शान्ति-संतोष की कमी अनुभव करते हुए चिन्ताग्रस्त एवं दु:खी ही बना रहा। यही कारण है कि मानव जीवन में प्रसन्नता का सतत अभाव होता जा रहा है।
इन समस्त दु:खों एवं अभावों से मनुष्य किस प्रकार मुक्ति पा सकता है, प्राचीन ऋषियों-मनीषियों एवं भारतीय तत्त्वदर्शी महापुरुषों ने इसके लिए कई प्रकार के मार्गों का कथन किया है, जो प्रत्यक्ष रूप से भले ही प्रतिकूल व पृथक् प्रतीत होते हों; परन्तु पात्र व रुचि के आधार पर सबका- अपना-अपना सच्चा दृष्टिकोण है। एक मार्ग वह है जो आत्मस्वरूप के ज्ञान के साथ-साथ भौतिक जगत् के समस्त पदार्थों के प्रति आत्मबुद्धि का भाव रखते हुए पारलौकिक साधनों का उपदेश देता है। दूसरा मार्ग वह है जो जीवमात्र को ईश्वर का अंश बतलाकर, जीवन में सेवा व भक्तिभाव के समावेश से लाभान्वित होकर आत्मलाभ की बात बतलाता है। तीसरा मार्ग वह है जो सांसारिक पदार्थों एवं लौकिक घटनाक्रमों के प्रति सात्विकता पूर्ण दृष्टि रखते हुए, उनके प्रति असक्ति न होने को श्रेयस्कर बताता है।
इसी तीसरे मार्ग का अवलम्बन न्यायदर्शन करता है, जबकि वह ईश्वरोपासना, पुनर्जन्म, लोक-परलोक, आत्मा आदि में भी भरपूर आस्था रखने वाली है, फिर भी इन सबकी सम्यक् उपलब्धि तथा इहलौकिक एवं परलौकिक जीवन की सफलता हेतु भौतिक जगत् के पदार्थों एवं उससे संबंधित घटनाओं का कथन करता है। न्याय का मानना है कि जो भी ज्ञान मनुष्य को उपलब्ध है, वह इन्द्रियों व मन-बुद्धि के माध्यम से ही प्राप्त हुआ करता है। इन सबमें विकृति उत्पन्न होने की स्थिति में उपलब्ध ज्ञान भी उसी अनुपात में विकारयुक्त हो जाने के कारण उस विकृत ज्ञान का आधार लेकर जो भी निर्णय लिया जायेगा तथा उससे किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति नहीं की जा सकेगी। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायशास्त्र ने यह सैद्धान्तिक अभिव्यक्ति की है कि संसार में न आने के पश्चात् यदि मनुष्य सत्कर्म व सद्व्यवहार के माध्यम से अपने दु:खों को दूर करना चाहे, तो सांसारिक संरचना में प्रयुक्त होने वाले जड़-चेतन सभी पदार्थों का वास्तविक स्वरूप भी जाने समझे। अनेक तरह के मतानुयायियों ने अपने अपने विचार से पदार्थों का स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार का बतलाया है, जिसके कारण मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। इस भ्रमात्मकतापूर्ण स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए न्यायशास्त्र ने तर्क व साक्ष्यों की ऐसी सुन्दर विचारधारा प्रस्तुत की है, जिससे पदार्थों के सही स्वरूप का निर्णय किया जा सके।
जिन साधनों से हमें ज्ञेय तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हीं साधनों को ‘न्याय’ की संज्ञा दी गई है। कहा भी है कि-
‘‘नीयते विवक्षितार्थ: अनेन इति
न्याय:।’’
न्यायदर्शन का इतिहास
गौतम के ‘न्याय सूत्र’ से ही न्यायशास्त्र का इतिहास
स्पष्ट
रूप से प्रारम्भ होता है। प्राचीन ग्रन्थों में इस न्यायशास्त्र के कतिपय
सिद्धान्तों की चर्चा तो आज भी विशद रूप से उपलब्ध है; परन्तु उस प्राचीन
तर्कशास्त्र का सम्यक् एवं सर्वांगपूर्ण स्वरूप क्या और कैसा था, इसका सही
ज्ञान किसी को नहीं है। ‘बौद्ध दर्शन’ के प्रकरणों
में यह
उल्लेख मिलता है कि बौद्ध मत वाले अपने मत का प्रतिपादन आस्तिक
सिद्धान्तों के विरुद्ध किया करते थे। इसी का प्रतिषेध करने हेतु
न्यायदर्शन की संरचना हुई। आगे इसका वर्णन किया जा रहा है। बुद्घ का समय
छठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यही वह समय था जब गौतम ने
न्यायशास्त्र की रचना की। न्यायदर्शन का एक नाम तर्कशास्त्र भी है।
प्राचीन ग्रन्थ शास्त्रों में किन्हीं-किन्हीं स्थानों में गौतम तथा
कहीं-कहीं अक्षपाद को न्यायदर्शन का रचयिता कहा गया है। आचार्य विश्वेश्वर
की तर्कभाषा की भूमिका के अन्तर्गत पृष्ठ 11-20 में इसका उल्लेख है। उमेश
मिश्र द्वारा रचित भारतीय दर्शन में कहा गया है कि तर्कशास्त्र बौद्धों के
पहले भी था और वह बड़ा व्यापक था। इसके भिन्न-भिन्न प्राचीन नाम हैं।
यथा-आन्तीक्षकी, हेतुशास्त्र, हेतुविद्या, तर्कशास्त्र, तर्कविद्या,
वादविद्या, प्रमाणशास्त्र, वाकोवाक्य, तक्की, विमंसि आदि।
रचनाकाल-
न्यायसूत्र की संरचना कब हुई, इसका निर्णय
कर पाना बहुत कठिन है।
कारण कि विद्वानों ने ई. पू. छठवीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व पाँचवी
शताब्दी के बीच अपनी मान्यतायें प्रस्तुत की हैं; परन्तु सबके अपने-अपने
पक्ष तर्कयुक्त हैं। उससे किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता।
भाष्य ग्रन्थ-
न्याय दर्शन के पश्चात् का जो साहित्य
उपलब्ध है, उन सबमें
‘न्याय भाष्य’ का प्रथम स्थान माना जाता है।
‘न्यायवार्तिक’ नाम की एक टीका न्यायभाष्य पर
‘उद्योतकर’ ने भी लिखी है, जिसमें न्यायशास्त्र के
प्रमेयों
के सही स्वरूप को जानने की सर्वाधिक उपादेयता विद्यमान है। इनका काल भी
ईसा की पाँचवीं-छठीं शताब्दी के आसपास ही है। उद्योतकर द्वारा रचित
‘न्यायवार्तिक’ नामक टीका प्रकाशित होने के पश्चात्
भी
न्यायशास्त्र पर बौद्धों का आघात बन्द नहीं हुआ, जिसके कारण ख्याति
प्राप्त टीकाकार पं. वाचस्पति को न्यायवार्तिक के ऊपर भी एक टीका लिखनी
पड़ी, जो ‘न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका’ के नाम से
प्रसिद्ध
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण टीका है। विद्वानों ने वाचस्पति मिश्र का समय ईसा की
नवीं शताब्दी मानी है। इन्होंने ही इस न्यायशास्त्र को शुद्ध एवं लिपिबद्ध
किया। इसी शुद्घता के कारण ही आज यह लेथा जोखा- उपलब्ध है कि न्यायदर्शन
में 5 अध्याय तथा 10 आह्निक हैं, 84 प्रकरण एवं 528 सूत्र हैं, 196 पद एवं
8385 अक्षर हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book